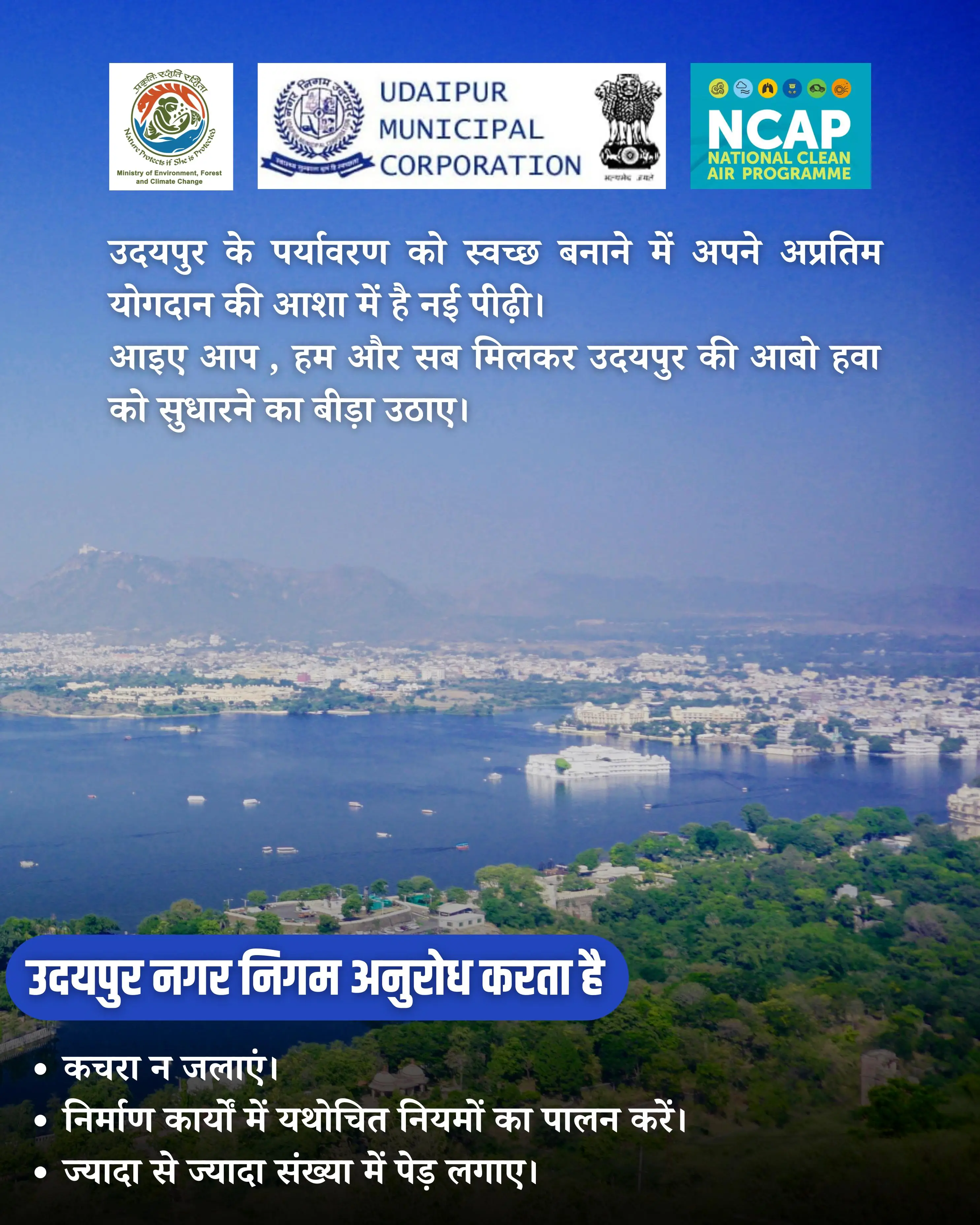उदयपुर के बारे में सबसे रोचक बात ये है कि इस ज़मीन पर इंसान 3000 ईसा पूर्व से रहता आया है जो कि उदयपुर जिले में स्थित आहड़ दक्षिणी पश्चिम राजस्थान की कांस्ययुगीन संस्कृति का मुख्य केन्द्रों में से एक था। यह संस्कृति बेडच बनास की घाटियों में विकसित हुई थी। आहड़, उदयपुर में आहड़ नदी के किनारे स्थित हैं। उदयपुर नाम रखने से पहले आहड़ सभ्यता के अन्य नाम है-आघाटपुर,ताम्रवती,धूलकोट और बनास संस्कृति। आप धूलकोट नाम से तो परिचित होंगे जो बोहरा गणेश मार्ग पर आहड़ संग्रहालय के पास स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जब इंसानी सभ्यता कपड़े पहनना सीख रही थी तब उदयपुर (आहड़) के लोग ताँबे और पाषाण के उपकरण काम में ले रहे थे। इस तरह 'ताम्रपाषण कालीन सभ्यता' का सबसे प्रमुख स्थल अगर कोई है तो वो उदयपुर है।
जावर माइंस क्षेत्र के आसपास भी कई हज़ारो साल पुरानी ताँबे और अन्य धातुओं को गलाने वाली भट्टियाँ उत्खनन मे आज भी मिलती है। मूलतः आहड़ सभ्यता के रूप में उदयपुर एक ग्रामीण संस्कृति का जीवन जी रहा था। यहाँ से एक मकान में 4-6 चूल्हे के प्रमाण मिले हैं,जिससे यह प्रतीत होता है कि आहड़ में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। यहाँ से अनाज के रूप में गेंहूँ, ज्वार और चावल के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से मिट्टी के पके हुए कोठे (अनाज संग्रह पात्र ) भी मिले हैं। आहड़ सभ्यता से प्राप्त बर्तनो का रंग लाल और काला होने के कारण इसे 'लाल और काले मृदभाण्ड वाली सभ्यता' भी कहते हैं।
यहाँ से बैल की मिट्टी की मूर्ति मिली है,जिसे बनासियन बुल भी कहते हैं। आहड़ से यूनानी मुद्रायें मिली है,जो प्रथम से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती हैं। पांच हज़ार साल पहले वर्तमान उदयपुर भूभाग पर रहने वाले लोग चूड़ियाँ ,छल्ले,सलाइयां ,ताँबे के दीपक ताँबे की कुल्हाड़ी का उपयोग किया करते थे जो ये बताता है कि उदयपुर का इतिहास मानव सभ्यता के विकास से शुरू होता है। बालाथल- वल्लभनगर (उदयपुर ),गिलूण्ड- राजसमन्द, ओझियाणा- भीलवाड़ा मेवाड़ के इतिहास की कहानी बताते है।
आयड नदी का इतिहास बहुत पुराना है और इसके किनारे किनारे 5000 से ज्यादा वर्ष पूर्व से सभ्यताएँ रहती आयी है। विभिन्न उत्खनन के स्तरों से पता चलता है कि प्रारम्भिक बसावट से लेकर 18 वीं सदी तक यहाँ कई बार बस्तियां बसी और उजड़ी। ऐसा लगता है कि आहड़ के आस-पास तांबे की उपलब्धता होने से सतत रूप से इस स्थान के निवासी इस धातु के उपकरण बनाते रहे और उन्हें एक ताम्रयुगीन कौशल केंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज भी उदयपुर बसने से पुर्व कई ग्राम बसे हुए थे जिनके अपने अवशेष मिलते है।
समय के साथ गांव बसते गए और दूर पहाड़ों पर ऐसे लोगों को भेज कर समाज निकाला कर दिया जाता था जिनका चाल चलन समाज के अनुरूप नहीं होता था। धीरे धीरे ये लोग सुदूर उदयपुर की पहाड़ियों में अपनी अलग बस्ती बनाने लगे। गुजरात सीमा तक ऐसे लोगों की बस्तियाँ कालान्तर में 4000 साल तक बसती रही। आदिवासी समाज के साथ साथ ग्रामीण सभ्यता उदयपुर में फलती फूलती रही। यहाँ जंगल ऐसे हुआ करते थे कि जमीन पर रोशनी तक नहीं आती थी और बाघ (शेर) से लेकर कई विलुप्त जंगली प्रजातियां यहाँ पायी जाती थी। आज भी कई अलग तरीके के जंगली वन्य जीव जैसे उड़न गिलहरी ,पेंगोलिन और विषैले कोबरा यहाँ कभी कभार देखने को मिल जाते है। सोचिये 500 साल पहले उदयपुर आना इतना दुर्गम था कि मुग़लों का यहाँ आने में पसीनें छूट गए थे। कई ऋषि मुनि यहाँ कालान्तर में निवास करते रहे और यही कारण है कि समूचे मेवाड़ में स्थानीय देवता के मन्दिर और देवरे यहाँ देखने को आम मिलते है।
मेवाड़ राज्य की स्थापना के लिए 565 ईस्वी में गुहादित्य ने गुहिल वंश की नींव रखी थी। मेवाड़ को मेदपाट/प्राग्वाट व शिवि जनपद के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र में मेद अर्थात् मेर जाति रहती थी। शिवि जनपद की राजधानी मध्यमिका/मझयमिका थी और मध्यमिका को वर्तमान में नगरी कहा जाता है जो चितौडग़ढ़ में स्थित है। मेद का शाब्दिक अर्थ - मलेच्छों को मारने वाला है। मेवाड़ के राजा स्वयं को राम का वंशज मानते थे। मेवाड़ राजाओं को ‘रघुवंशी’ या ‘हिन्दुआ सूरज’ भी कहा जाता है। मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी।
संसार में एक ही क्षेत्र में अधिक समय तक राज करने वाला एकमात्र राजवंश मेवाड़ राजवंश है| राजस्थान में मेवाड़ सबसे प्राचीन राजवंश था। 565 ई में गुहादित्य ने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। मेवाड़ में गुहिल वंश के संस्थापक गुहादित्य ने 565 ईस्वी में गुहिलवंश की नींव रखी।
मेवाड़ में गुहिल वंश का प्रथम प्रतापी राजा बप्पा रावल (734 ई.-753 ई.) थे । बप्पारावल को कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। बप्पारावल को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बप्पारावल हारित ऋषि की गाय को चराते थे। मेवाड़ के राजा एकलिंग नाथ के दीवान के रूप में शासन करते है। 734 ई. में बप्पारावल ने मौर्य शासक मानमौरी से चितौडग़ढ़ का किला जीता तथा नागदा (उदयपुर के एकलिंग जी के पास स्थित) को राजधानी बनाया। नागदा मेवाड़ के गुहिल वंश की प्रारम्भिक राजधानी थी जो कैलाशपुरी से मात्र 6 किमी दूर है। बप्पा रावल की समाधि भी नागदा उदयपुर में बनी है। इसके बाद अल्लट (951-953ई०) ने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की शुरूआत महाराणा अल्लट ने ही की थी। महाराणा जैत्रसिहं के समय इल्तुतमिश 1222-29 ई० के बीच ने नागदा पर आक्रमण किया। महाराणा जैत्रसिंह ने नागदा से राजधानी हटाकर चितौड़ को राजधानी बनाया। महाराणा तेजसिंह ने 1260 ई० में मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम ग्रन्थ "श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णि" (कमल चंद्र द्वारा रचित) तेजसिंह के काल में लिखा गया है। मेवाड़ के कुलदेवता एकलिंगनाथ जी का मन्दिर बप्पारावल ने कैलाशपुरी (उदयपुर) में बनवाया था।
कैसे गुहिल वंश से सिसोदिआ वंश में तब्दील हुआ मेवाड़ का राजपरिवार ?
गुहिल वंश के राजा राहप ने उदयपुर के सिसोदा ग्राम में जाकर रहना शुरू किया। राहप के ही वंश में लक्ष्मण देव सिसोदिया हुआ। रावल रत्नसिंह मेवाड़ के गुहिल या रावल वंश का अंतिम राजा थे ।1303 ई० में चितौडग़ढ़ में रावल रत्न सिंह का शासन था। 28 जनवरी 1303 ई० में अलाउद्दीन खिलजी ने चितौड़ पर आक्रमण किया व 26 अगस्त 1303 ई० को चितौडगढ़ के किले को जीत लिया । इस युद्ध में रावल रत्न सिंह व उसकी सेना के साथ दो वीर सैनिक गौरा व बादल मारे गए तथा रानी पद्मिनी ने जौहर किया(गौरा पद्मिनी का चाचा था व बादल चचेरा भाई था।)। इसे चितौड़ का पहला साका कहते है। अलाउद्दीन खिलजी ने चितौड़ को 8 माह तक घेरे रखा। अलाउद्दीन खिलजी के पास पत्थर फेंकने के उपकरण थे। जिसकी सहायता से चितौडगढ़ पर पत्थर फेंके गए। चितौड़ के पहले साके में इतिहासकार अमीर खुसरो मौजूद था जिसने इस साके का वर्णन अपनी रचना "खजाइनुल कुतुह या तारीख-ए-अलाई" में किया है। चितौडग़ढ़ दुर्ग जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम खिज्राबाद रखा। 1303 ईस्वी में अल्लाउददीन खिलजी ने 5 साल बाद दूसरी बार चित्तौड़ पर हमला किया। चित्तौड़ की पहली घेराबंदी के दौरान अधिकांश लड़ाई करने वाले पुरुष चारो ओर से गिर गए थे। मेवाड़ की आन-बान को बचाने के प्रयास में सभी राजपूत पुरुष अंतिम चरण के दौरान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इस बीच रानी पद्मिनी ने सभी राजपूत महिलाओं के साथ जौहर कर आत्मदाह कर लिया। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बच गई महिलाओं पर कब्जा कर लिया। मेवाड़ राजवश से जुड़े परिवार के कुछ युवा लड़के हमले के दौरान किले में नहीं थे इसलिए वंश बच गया।
बचे हुए लोगों में हम्मीर था जो सिसोदा गाँव का रहने वाला था। हमीर की रानी और मल देव सोंगिरा की बेटी ने उन्हें चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करने में मदद की। अंततः राणा हमीर ने 16 साल के मुस्लिम कब्जे के बाद चित्तौड़ पर फिर से शासन किया। "सिसोदा" के उनके गांव के बाद उनके वंश का नाम सिसोदिया रखा गया। लक्ष्मण देव सिसोदिया के सात पुत्रों में से छ: पुत्र चितौड़ के पहले साके (1303) में मारे गऐ तथा सातवां पुत्र हम्मीर सिसोदिया ने मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की नींव रखी। राणा हम्मीर ने दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद तुगलक के चितौडगढ पर आक्रमण को विफल कर दिया। राणा कुंभा द्वारा रचित रसिकप्रिया (जयदेव की गीतगोविन्द पर टीका) तथा अत्रि व महेश द्वारा विजय स्तम्भ पर लिखी गयी कीर्तिस्तम्भ प्रशस्ति (1460) में राणा हम्मीर को विषमघाटी पंचानन (युद्ध में सिंह के समान) बताया गया है। चितौड़ का नाम धाई बा पीर की दरगाह के अभिलेख में मिलता है। राणा कुम्भा ने अचलगढ़ दुर्ग (सिरोही) का पुन:निर्माण करवाया, बंसतीगढ दुर्ग (सिरोही), भीलों से सुरक्षा हेतु भोमट दुर्ग (सिरोही) तथा मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए बैराठ दुर्ग (बदनौर, भीलवाड़ा) का निर्माण करवाया। भोमट क्षेत्र भीलों का निवास क्षेत्र कहलाता है।
कुम्भा ने संगीतराज, संगीतसार, संगीत मीमांशा, सूढ प्रबंध व रसिकप्रिया (जयदेव की गीत गोविन्द पर टीका) आदि ग्रंथों की रचना की। कुंभा द्वारा लिखे गए संगीत ग्रंथों में सबसे बड़ा ग्रंथ संगीतराज है। कुंभा का संगीत गुरू सारंगव्यास था तथा चित्रकला गुरू हीरानंद था। हीरानंद ने 1423 ई में (राणा मोकल के समय) मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण ग्रंथ ‘सुपास नाहचरियम’ की रचना की। कुम्भा की पुत्री रमाबाई संगीत की विदुषी थी जिसे वागेश्वरी की उपाधि प्राप्त थी। कुम्भा का दरबारी कवि कान्हव्यास था जिसने एकलिंगनाथ माहात्मय (संस्कृत भाषा) की रचना की। एकलिंग महात्मय संगीत के स्वरों से संबंधित ग्रंथ है। जिसका प्रथम भाग राजवर्णन कुम्भा द्वारा लिखा गया है। राणा कुम्भा के समय 1439 ई० में पाली में राणकपुर के जैन मन्दिर (कुम्भलगढ अभयारण्य) में का निर्माण धरणक सेठ द्वारा करवाया गया इन मंदिरों का शिल्पी देपाक/ देपा था।रणकपुर के जैन मंदिर मथाई नदी के किनारे स्थित है। रणकपुर के जैन मन्दिरो को चौमुखा मन्दिर भी कहते है। यह मन्दिर प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ (ऋषभदेव) को समर्पित है। रणकपुर के जैन मन्दिर में 1444 खम्भे है। अत: इन्हें वनों का मन्दिर या खम्भों का मन्दिर या स्तम्भों का वन भी कहते है। राणा कुम्भा द्वारा बदनौर (भीलवाड़ा) में कुशाल माता का मंदिर बनवाया गया। कुंभा ने चितौडगढ़ दुर्ग का पुन: निर्माण करवाया। कुंभा धर्म सहिष्णु शासक था। उन्होंने आबू पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों से लिया जाने वाला कर भी समाप्त कर दिया था।
पिछोली गांव भी उदयपुर के बसने से पहले का है यह काल महाराणा लाखा का काल था ( 1382 से 1421)। कुछ बंजारे जिसमे छीतर नाम का बनजारा भी था और वे जब वर्तमान के पिछोला से गुजर रहे थे तब उनकी बैलगाड़ी नमी वाली जगह में धस गई उस समुह ने पानी का स्त्रोत जानकर खुदाई की और फलस्वरूप पिछोला झील का निर्माण हुआ यहां चारों तरफ पहाड़ी इलाके थे।
इसके बाद महाराणा लाखा/लक्षसिंह (1382-1421) का राज आया और राणा लाखा का विवाह मारवाड़ के रणमल की बहिन हंसाबाई से हुआ। राणा मोकल इन्ही की संतान थी जिसने बाद में मेंवाड़ का शासन सम्भाला। राणा मोकल ने चितौडगढ़ में समिद्वेश्वर मंदिर (त्रिभुवन नारायण मंदिर) का पुननिर्माण करवाया था। समिद्वेश्वर मंदिर का निर्माण पूर्व में परमार राजा भोज ने करवाया। राणा लाखा का पुत्र राणा चुण्डा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। रघुकुल वंश श्री रामचंद्र के बाद पितृ भक्ति का ज्वलंत उदाहरण राणा चूंडा का मिलता है। राणा लाखा के समय 1387 ई० में छित्तरमल नामक बनजारे ने पिछोला झील (उदयपुर) का निर्माण करवाया । सीसे जस्ते (जुड़वा खनिज)की प्रसिद्ध खान जावर खान (उदयपुर) की खोज भी राणा लाखा के समय हुई थी।
राणा कुम्भा (1433-1468 ई०) का जन्म 1423 ई० में चितौडगढ़ दुर्ग में हुआ। राणा कुंभा का राज्यभिषेक 10 वर्ष की आयु में 1433 ई० में चितौडगढ़ दुर्ग में हुआ। राजस्थान में कला व स्थापत्य कला की दृष्टि से राणा कुंभा का काल स्वर्ण काल कहलाता है। राणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहते है। कुंभा के पिता का नाम मोकल व माता का नाम सौभाग्यदेवी था। राणा कुंभा को हाल गुरू (गिरी दुर्गों का स्वामी), राजगुरू (राजनीति में दक्ष), राणारासो,अभिनव भरताचार्य ,नाटकराजक(कुंभा ने 4 नाटक लिखे), प्रज्ञापालक, रायरायन, महराजाधिराज, महाराणा, चापगुरू (धनुर्विद्या में पारंगत ),शैलगुरू, नरपति,परमगुरू,हिन्दू सूत्राण,दान गुरू,तोडरमल (संगीत की तीनों विधाओं में श्रेष्ठ), नंदनदीश्वर(शैव धर्म का उपासक) आदि उपाधियां प्राप्त थी। राणा कुंभा को अश्वपति, गणपति, छाप गुरू (छापामार पद्धति में कुशल) आदि सैनिक उपाधियां भी प्राप्त थी। मेवाड़ के राणा कुम्भा व मारवाड़ के राव जोधा के बीच आवल-बावल की संधि हुई। इस संधि के द्वारा मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया तथा जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह राणा कुम्भा के पुत्र रायमल से किया। इसकी जानकारी श्रृंगारी देवी द्वारा बनाई गयी घोसुण्डी की बावड़ी (चितौडग़ढ) पर लगी प्रशस्ति से मिलता है।
1437 ई० में राणा कुम्भा व मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के बीच सारंगपुर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा कुम्भा विजयी हुआ तथा युद्ध विजयी की खुशी में चितौडग़ढ़ दुर्ग में विजय स्तम्भ का निर्माण करवाया। विजय स्तम्भ भगवान विष्णु को समर्पित है अत: इसे विष्णु ध्वज या विष्णु स्तम्भ भी कहते है। विजय स्तम्भ के शिल्पी जैता, नापा और पुंजा थे। विजयस्तम्भ 122 फीट ऊँचा व 9 मंजिला इमारत है। इसमें 157 सीढ़ीयां है और यह राणा कुंभा के समय की सर्वाेतम कलाकृति है। विजय स्तंभ बनाने में उस समय कुल 90 लाख रूपये खर्च हुए। कर्नल टॉड ने विजय स्तंभ को कुतुब मिनार से बेहतरीन इमारत बताया है तथा फग्र्यूसन ने विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से की है।
कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा द्वारा अपनी पत्नी कुंभलदेवी की याद में 1443-59 ई० के बीच बनवाया गया। कुंभलगढ़ दुर्ग को कुंभलमेर दुर्ग,मछींदरपुर दुर्ग,बैरों का दुर्ग, मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, कुंभपुर दुर्ग, कमल पीर दुर्ग भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग में कृषि भूमि भी है। अत: कुंभलगढ़ दुर्ग को राजस्थान का आत्मनिर्भर दुर्ग कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग में 50 हजार व्यक्ति निवास करते थे। कुंभलगढ़ दुर्ग हाथी की नाल दर्रे पर अरावली की जरगा पहाड़ी पर कुंभलगढ़ अभयारण्य में राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर भारत में सभी दुर्गों की प्राचीर से लम्बी है। इसकी प्राचीर 36 किमी० लम्बे परकोटे से घिरी है। अत: इसे भारत की मीनार भी कहते है। इसकी प्राचीर पर एक साथ चार घोड़े दौड़ाए जा सकते है।कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा है कि ‘यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है।’कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की दृढ़ता के कारण इसको ‘एट्रूस्कन’ दुर्ग की संज्ञा दी है।
1456 ई० में गुजरात के कुतुबद्दीनशाह व मालवा शासक महमूद खिलजी प्रथम के बीच कुम्भा के विरूद्ध चम्पानेर की संधि हुई। इस संधि में तय किया गया कि दोनों मेवाड़ के राणा कुंभा को मारकर मेवाड़ आपस में बांट लेंगे। लेकिन कुम्भा ने इस संधि को विफल कर दिया। कुम्भगढ़ दुर्ग में सबसे ऊँचाई पर बना एक छोटा दुर्ग कटारगढ़ है। जहाँ से पूरा मेवाड़ दिखाई देता है अत: कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहते है। कटारगढ़ दुर्ग/मामदेव मंदिर कुम्भा का निवास स्थल था तथा इसी दुर्ग में कुम्भा के पुत्र ऊदा/उदयकरण ने कुम्भा की हत्या की। कुंभलगढ़ दुर्ग में पन्नाधाय उदयसिंह को बचा कर लाई थी तथा कुम्भगढ दुर्ग में ही 1537 ई० में उदयसिंह का राज्यभिषेक हुआ। कटारगढ़ दुर्ग (कुंभलगढ़ दुर्ग) में 9 मई 1540 ई० को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। हल्दीघाटी युद्ध (1576 ई०) के बाद 1578 ई० ई में महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया तथा यहीं महाराणा प्रताप का 1578 ई० में दूसरा व औपचारिक राज्यभिषेक हुआ।
मतभेद: : देपाक या देपा द्वारा रचित रणकपुर प्रशस्ति (1439 ई०) में बप्पारावल व कालभोज को अलग-अलग व्यक्ति बताया गया है। विजय स्तंभ पर लिखी गई कीर्तिस्तम्भ प्रशस्ति (अत्रि व उसके पुत्र महेश द्वारा रचित)1460 ई०में बप्पारावल से कुंभा तक के राजाओं की उपलब्धियों व युद्ध विजयों का वर्णन है। संस्कृत भाषा में लिखित इस प्रशस्ति में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों का वर्णन किया गया है। कुम्भलगढ़ प्रशस्ति (महेश द्वारा रचित 1460 ई०) में बप्पा रावल को ब्राह्मण या विप्रवंशीय बताया है। 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण कुंभश्याम मंदिर/मामदेव मंदिर में संस्कृत भाषा में लिखी है।एकलिंग नाथ के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति 1488 ई० में बप्पा रावल के संन्यास लेने का उल्लेख है। संग्राम सिंह द्वितीय के काल में 1719 ई० में लिखी गयी वैद्यनाथ प्रशस्ति में हारित ऋषि से बप्पा रावल को मेवाड़ साम्राज्य मिलने का उल्लेख है। वैद्यनाथ प्रशस्ति रूप भट्ट द्वारा लिखित पिछोला झील के निकट सीसा रास (वर्तमान सीसारमा) गांव के वैद्यनाथ मेंदिर में स्थित है।
कालान्तर में जब महाराणा उदय सिंह जी का चित्तौड़गढ़ निरन्तर आक्रमण झेल रहा था। उन्ही दिनों महाराणा उदय सिंह जी अपने पौत्र कुंवर अमरसिंह के जन्म के उपलक्ष्य में एकलिंग जी मन्दिर दर्शन को आए फिर शिकार के लिए आयड गांव में डेरे डलवाए। लेकिन दिमाग में निरन्तर चित्तोड पर मुग़ल आताताइयों के आक्रमण से दिमाग में एक योजना चल रहीं थी कि एक सुरक्षित राजधानी बनाई जाए ताकि स्थिरता आ सकें।
उन्ही दिनों की एक शाम में सभी सामंत और मुख्य व्यक्तियों के सामने महाराणा ने उदयपुर नगर बसाने का विचार रखा। सामंतों मंत्रीयो ने सुझाव का समर्थन किया और जगह की तलाश करवाई गई फलस्वरूप मोतीमहल जिसके खण्डर वर्तमान में मोतीमगरी पर है, महल तैयार किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि मोतीमहल उदयपुर का पहला महल था और एक तरह से यह नए उदयपुर नगर की शुरूआत थी।
उदयपुर स्थापना का दिन 15 अप्रैल 1553 है जो इतिहास कारों द्वारा मान्य है और उस दिन आखातीज का दिन था । यही दिन उदयपुर स्थापना दिवस माना गया यह सभी वर्तमान इतिहास कारों ने सहमति से माना है क्योंकि कही भी उदयपुर स्थापना दिवस का शिलालेख या अन्य कोई प्रमाण नहीं मिलता है।
एक बार महाराणा उदय सिंह जी मोतीमहल मे निवास कर रहे थे तब शिकार कि भावना से खरगोश का पीछा करते हुए वर्तमान फतहसागर जो की उस समय वजूद मे नही था और केवल एक सहायक नदी रूप था। नदी किनारे घोड़ा दोडाते हुए वर्तमान चांदपोल के रास्ते उदयपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी जहां वर्तमान में राजमहल है वहां पहुंच कर विश्राम लिया। तभी वहां पहाड़ी पर एक साधु की धुणी से धुआं उठते देख महाराणा वहां पहुंचे। वहां पर योगी धुणी पर विराजमान सन्त का नाम जगतगिरी जी जो कि बहुत पहुँचे हुए संत थे, उन्होंने महाराणा के दिल का हाल जानकर जहां धुणी थी वहीं राज्य बसाने का आदेश दिया।
यह धुणी वर्तमान मे भी राजमहल में स्थित है और कोई भी महाराणा उदयपुर की सत्ता संभालने पर इस धुणी पर आशिर्वाद लेने निश्चित रूप से जाते है। यह एक उदयपुर स्थापना से लगाकर वर्तमान महाराणा महेंद्र सिंह जी तक यह दस्तुर चला आ रहा है।
आज भी राजमहल उदयपुर शहर की सबसे बड़ी चोटी पर है जो शहर मे हर तरफ से दिखता है और यह भव्य राजमहल कई चरणों में अलग-अलग महाराणा के काल में बना। बाद मे कालान्तर में सरदार राव उमराव पासवान सभी को राजमहल के नजदीक बसाया। जितने भी जागिरदार उमराव सरदारों की हवेली है, वे राजमहल के निकट घाटीयो पर ही बसी है।
शोधकर्ता :
दिनेश भट्ट
नोट : उपरोक्त तथ्य लोगों की जानकारी के लिए है और काल खण्ड ,तथ्य और समय की जानकारी देते यद्धपि सावधानी बरती गयी है , फिर भी किसी वाद -विवाद के लिए अधिकृत जानकारी को महत्ता दी जाए। न्यूज़एजेंसीइंडिया.कॉम किसी भी तथ्य और प्रासंगिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है।